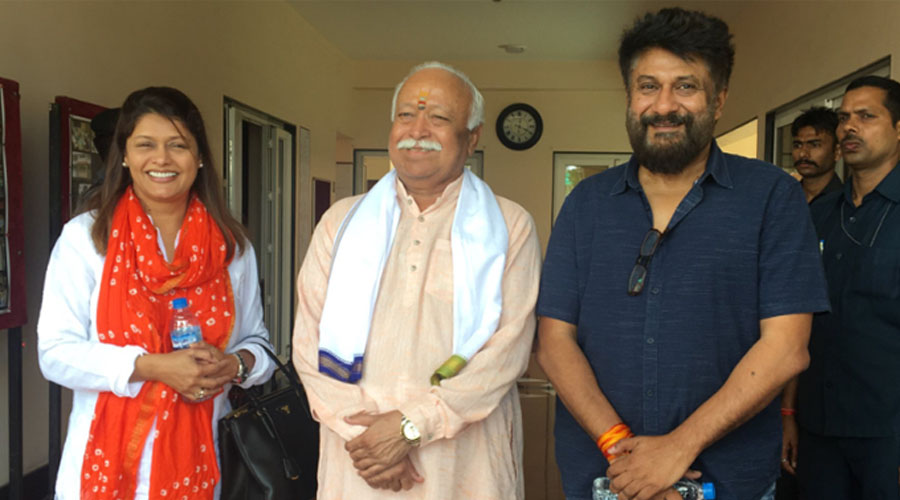फ़िल्म की आड़ में जिस तरह सिनेमाघरों में उन्मादी भाषण दिए जा रहे हैं, साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक, सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक फ़िल्म को जिस परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं उससे फ़िल्म का मकसद क्या है ये समझना मुश्किल नहीं।
ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। मुख्य धारा की मीडिया हो या सोशल मीडिया, नुक्कड़ की चाय की दुकान हो या देश की पार्लियामेंट लोग हर जगह बोल रहे हैं। साधारण नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक बोल रहे हैं। जो नहीं बोल रहा उससे कहा जा रहा तुम बोल क्यों नहीं रहे। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर फाइल्स की। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी यह फ़िल्म आज हर जगह चर्चा का विषय है। मैं कभी कश्मीर नहीं गया। कश्मीर के बारे में मेरी जो भी समझ है या मैंने कश्मीर को जितना भी समझने की कोशिश की है वो कुछ किताबों के जरिये, कुछ संस्मरणों के जरिये, कुछ वहाँ के और उन परिस्थितियों से जुड़े हुए लोगों के साक्षात्कार के जरिए और कुछ हद तक सिनेमा के जरिए भी। कश्मीर को लेकर पहली बार उत्सुकता तब जगी जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उससे पहले कश्मीर के बारे में उतना ही जानता था जितना कि मुख्यधारा की मीडिया ने दिखाया था। कश्मीर के बारे में जैसे जैसे पढ़ता गया ये महसूस हुआ कि मैं कश्मीर को कितना कम जानता हूँ और कश्मीर को लेकर मेरी बुनियादी समझ कितनी कम है फिर भी अपनी सीमित जानकारी के साथ कुछ लिखने का प्रयास जरूर करूंगा।
दंगे एक सच्चाई हैं। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर, कहीं नस्ल के नाम पर तो कहीं भाषा के नाम पर। लगभग सभी जानकार ये मानते हैं कि 80 के शुरुआती दशक तक कश्मीर अपेक्षाकृत एक शांत प्रदेश था लेकिन अगर आप राहुल पंडिता की ‘अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट’ पढेंगे तो पता चलेगा कि इसका बीज काफी पहले रोपा जा चुका था।
बकौल राहुल पंडिता मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच एक लाइन खींची जा चुकी थी जो आगे चलकर एक गहरी खाई में तब्दील हो गई। कश्मीरी मामलों के लगभग सभी जानकार ये मानते हैं कि 1987 के कश्मीर चुनावों में हुई धांधली कश्मीर में पनपते उग्रवाद के लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हुई। कश्मीर के अलगाववादी वहाँ के युवाओं को ये समझाने में कामयाब हुए कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों को नहीं हासिल किया जा सकता और इसके बाद ही हर उस इंसान को निशाना बनाया गया जो भारत या भारतीय सरकार की नुमाइंदगी करते थे।
अगर समाज का एक हिस्सा ये मानने लगे कि वो अब इस समाज का हिस्सा नहीं और उसकी एक्टिविटी कहीं और से कंट्रोल होने लगे तो एक सरकार और एक समाज के तौर पर ये देश की बहुत बड़ी असफलता है।
राजेश भट्ट की किताब ‘रेडियो कश्मीर’ के अनुसार कश्मीर दूरदर्शन में काम करने वाले कई लोगों का कत्लेआम हुआ जिसमें हिन्दू भी थे और मुसलमान भी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के अलगाववादी संगठनों को ये अंदेशा था कि रेडियो कश्मीर के माध्यम से वहाँ भारतीय सरकार का एजेंडा चलाया जा रहा है। ए. एस दुल्लत साहब ने अपनी किताब ‘कश्मीर द वाजपेयी ईयर’ में लिखा है कि इस दौर में आई बी के कई अधिकारियों का अपहरण और कत्लेआम हुआ जिसमें हिन्दू भी थे और मुसलमान भी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आई बी भारतीय सरकार को कश्मीर की खुफिया जानकारी दे रही थी जो पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों को कत्तई पसंद नहीं था।

कश्मीर में उग्रवाद का विस्फोट हुआ 12 दिसंबर 1989 को, जब देश के तत्कालीन गृहमंत्री मुफ़्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉ रुबिया सईद का अपहरण कर लिया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला के विरोध के बावजूद 5 खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया गया जिससे आगे चलकर कश्मीर घाटी में आतंकवाद की आग धधक उठी। सैफ़ुद्दीन सोज़ ने अपनी किताब ‘कश्मीर:ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ स्ट्रगल’ में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि मुफ़्ती मोहम्मद सईद का वी.पी सिंह की सरकार में वही रुतबा था जो वर्तमान सरकार में अमित शाह का है। इस सरकार को लेफ्ट और बीजेपी का भी समर्थन प्राप्त था। मूसा रजा जो मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्ला के मुख्य सचिव थे उन्होंने अपनी किताब ‘कश्मीर अ लैंड ऑफ रिग्रेट’ में भी इस घटना का जिक्र किया है। वज़ाहत हबीबुल्लाह ने अपनी किताब ‘माई कश्मीर: द डाइंग ऑफ अ लाइट‘ में लिखा है कि नई सरकार आतंकियों के दबाव में झुक गई और फ़ारूक़ को अनसुना कर दिया गया।
ये सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ पोलिटिकल पार्टीज से जुड़े मुस्लिम भी उस दौर में आतंकवाद का शिकार बने लेकिन सच ये भी है कि कश्मीरी पंडितों की तरह वहाँ रह रहे मुस्लिम समुदाय को पलायन नहीं करना पड़ा।
हालांकि बशरत पीर की किताब ‘कर्फ्यू नाईट’ के अनुसार पलायन मुस्लिम युवकों का भी हुआ लेकिन वो बेहतर अवसर और बेहतर जीवन प्रत्याशा के लिए था। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सच ये भी है कि बहुसंख्यक मुस्लिम समाज ने इस दौर में पंडितों को अकेला छोड़ दिया।
सच ये भी है कि उस समय की सरकारों ने अव्वल दर्जे का नाकारापन दिखाते हुए उभरती हुई मिलिटेंसी को रोकने का कोई खास प्रयास नहीं किया।इतनी प्रताड़ना के बाद भी किसी कश्मीरी पंडित नें हथियार नहीं उठाया, सच ये भी है। बिना किसी गलती के सिर्फ नफरत की बुनियाद पर किसी को बेघर करने को आप किसी तरह जायज नहीं ठहरा सकते चाहें आप कितनी ही दलीलें क्यों न दें। रातोंरात अगर आपको अपना सब कुछ छोड़कर किसी रिफ्यूजी कैम्प में जिंदगी बितानी पड़े इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती।
ज़िन्दगी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में आप सबसे अकेले होते हैं। टूटने की हद तक। तब लगता है किसी चीज़ के कोई मायने ही नहीं। अस्तित्व का संकट ही आपको खाये जा रहा है, ये ऐसा वक़्त होता है जब चाहकर भी कोई साथ नहीं दे सकता। वो अपना हाथ बढ़ा रहे होते हैं, पर उनका हाथ हमें बचा नहीं सकता। बहुसंख्यक समाज की ये जिम्मेदारी है कि अपने साथ रहने वाले अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक न महसूस होने दे। ये बात कश्मीर पर भी लागू होती है और शेष भारत पर भी।
कश्मीर फाइल्स देखते हुए आप ये महसूस करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को उकेरते हुए एक खास समुदाय को खलनायक बनाना फ़िल्म का मुख्य मकसद है। किसी फिल्म में क्या दिखाया जाए और क्या न दिखाया जाए ये फ़िल्म के निर्माता निर्देशक का विशेषाधिकार है लेकिन फ़िल्म की आड़ में जिस तरह सिनेमाघरों में उन्मादी भाषण दिए जा रहे हैं, साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक, सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक फ़िल्म को जिस परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं उससे फ़िल्म का मकसद क्या है ये समझना मुश्किल नहीं।
सच को अगर बहुत समय तक न कहा जाए तो उस पर फफूंद लग जाती है। सच कहा जाना चाहिए सच लिखा जाना चाहिए, सच दिखाया भी जाना चाहिए और उस सच को कसौटी पर कसा भी जाना चाहिए। फ़िल्म के अनुसार करीब 4000 कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ जबकि कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार करीब 600 पंडितों का। गृह मंत्रालय इन आंकड़ों की संख्या 219 बताता है। इसमे से किन आंकड़ों को आप ज्यादा प्रासंगिक मानते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं पर अगर आप वास्तव में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मनोज जोशी की ‘द लॉस्ट रिबेलियन’ पढ़नी चाहिए।

कश्मीर फाइल्स को लेकर जो माहौल बनाया गया है उसके अनुसार जो फ़िल्म में दिखाया गया है वही अंतिम सत्य है और इससे इतर राय रखने वालों के लिए कहीं कोई जगह नहीं। चाहे वो इस त्रासदी से गुज़रे हुए लोग ही क्यों न हो। राहुल पंडिता की ट्विटर टाइम लाइन को अगर आप देखेंगे तो आपको मेरी बातें पुख्ता लगेगी। राहुल पंडिता जो खुद इस त्रासदी के शिकार हैं और इस पर एक फ़िल्म ‘शिकारा’ की कहानी भी लिख चुके हैं को थोड़ी अलग राय रखने की वज़ह से बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।
पक्ष और पार्टी से परे सारी सरकारों ने कश्मीरी पंडितों को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। बार बार उन जख्मों को कुरेदा गया पर मरहम किसी ने नहीं लगाया। 30 साल से ज्यादा हो गए वो अभी भी जम्मू और देश के दूसरे इलाकों में विस्थापितों की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं। उन्हें न्याय मिलना चाहिए पर क्या वो न्याय भीड़ करेगी? जवाब है नहीं। एक कमेटी गठित होनी चाहिए जिसकी सुनवाई फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट में हो और एक नियत समय में इसकी जांच पूरी करके दोषियों को सजा मिले जिससे ये नज़ीर बन सके कि कश्मीर ही नहीं देश के किसी भी हिस्से में यदि बहुसंख्यक समाज धर्म जाति या नस्ल के नाम पर किसी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव करे तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही पीड़ित पक्ष के साथ न्याय होगा।
(यह लेखक के निजी विचार हैं।)